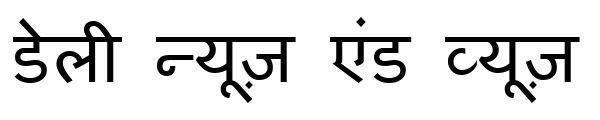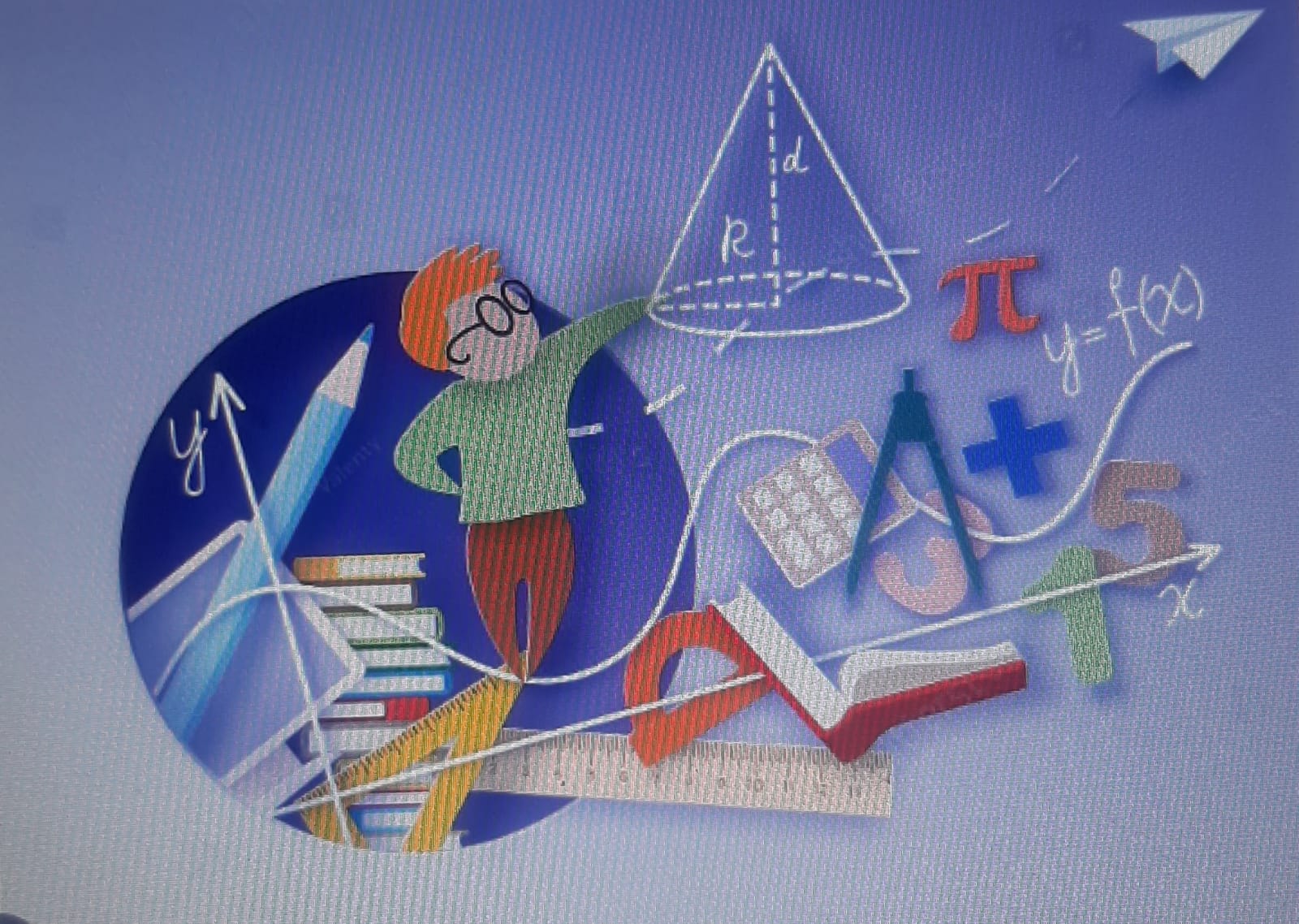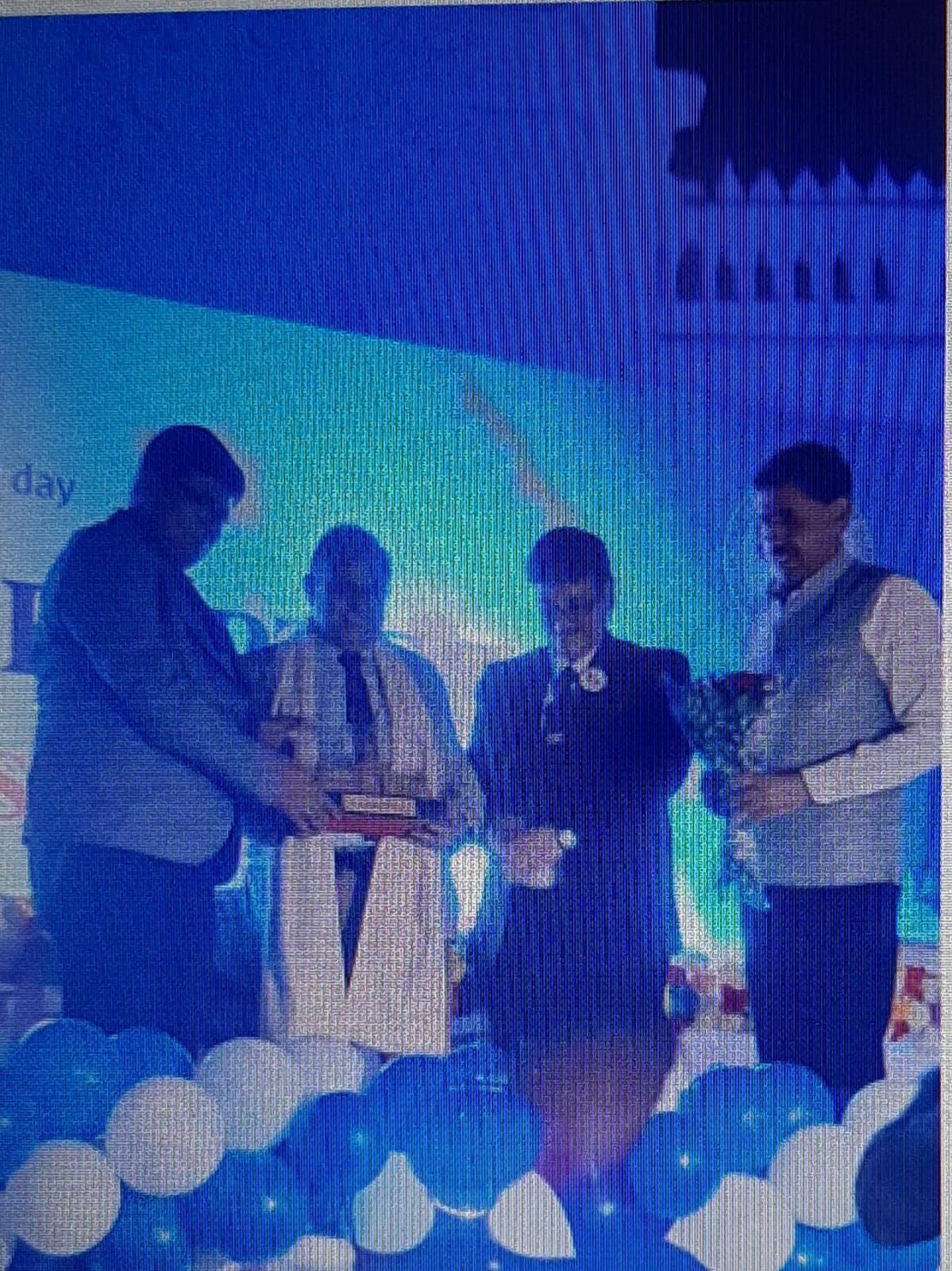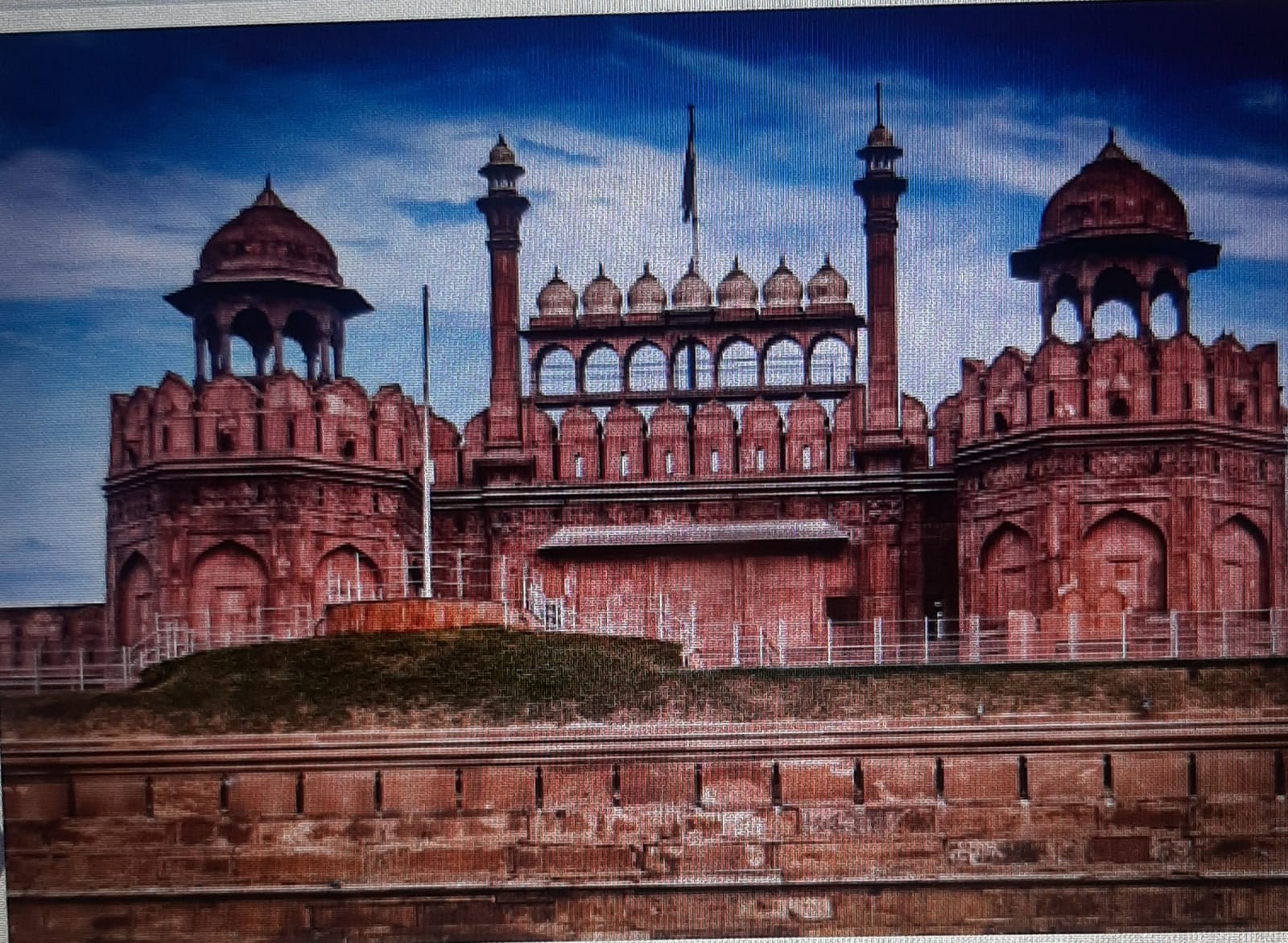दुर्भाग्यवश,देश में दिखावे की परंपरा प्रभावी रही है,तथा आज शिक्षा-क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है।दुख इस बात का है कि नीति-निर्धारकों से लेकर नीति-अनुपालनहार तक,कहीं भी इस परंपरा के विरोध में आवाज़ नहीं उठ रही है।शिक्षा की आत्मा को समझिये,यह देश व समाज के विकास का अस्त्र है तथा इसे शानदार भवन व महँगे उपकरणों के मखमली म्यान में रख कर इसकी धार कुन्द न कीजिये।
प्रो. एच सी पांडे
अकबर इलाहाबादी ने फ़रमाया था:
रेज़ोल्यूशन्स की शोरिश है,पर उनका असर ग़ायब ,
पलेटों की सदा सुनता हूँ ,मगर खाना नहीं आता।
सन १९२४ के सर जॉन सारजेंट आयोग से लेकर कोठारी आयोग और न जाने कितने आयोग,शिक्षा नीति पर अपनी अंनुसंशायें दे चुके हैं पर किसी भी आयोग की सिफ़ारिशों को,कोई भी सरकार,पूरी तरह लागू नहीं कर पाई।हॉं,रस्में-अयादगी ज़रूर हुई।अनुशंसाओं को क्रान्तिकारी बताया गया और शिक्षा स्तर के आसमान छूने पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया,नये नामकरण हुवे और नाम-पट्ट बदले और बस,शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो गया!
नयी शब्दावली से वास्तविकता नहीं बदलती और न अधूरी सिफ़ारिशों को, ढिलाई से लागू करने से,कोई चमत्कार होता है।हॉं,इतना अवश्य होता है कि समस्या वहीं की वहीं रहती है,जिस से अगली सरकार को,एक और आयोग बनाने का औचित्य मिल जाता है।
किसी भी कार्यक्रम की नियति उसके सूत्रधार की नियत पर निर्भर रहती है।काम करना है,तो काम होगा पर अगर दिखावा है तो फिर कोई भी नीति बेमतलब है।माना कि आज के राजनैतिक जीवन में बने रहने के लिये दिखावा ज़रूरी है,और दिखाने के दाँत भी चाहिये,पर हाथी के खाने के दाँत भी होते हैं तभी तो वह जीवित रहता है।आधुनिक विचारों की टाई लगाने से पहले बुनियादी यथार्थ की धोती कसनी भी ज़रूरी है। नीति,देश की समस्याओं व लक्षों के परिपेक्ष में बनती है,तथा,उपलब्ध साधनों की सीमाओं में ही लागू की जा सकती है।ज्ञान के असीमित आकाश में उड़ान अंतहीन है पर आज के भारत को यथार्थ के धरातल पर रहना होगा।फ़्रांसिस बेकन के अनुसार उपार्जित विद्या कार्य करने के लिये है न कि संचय करने के लिये।आइंस्टाइन के शब्दों में शिक्षा मूल उद्देश्य है “स्वतंत्र विचार तथा कार्य करने वाले व्यक्तियों को दीक्षित करना जो समाज की सेवा को जीवन का उच्चतम लक्ष मानें”।अत: छात्रों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व,तथा,अर्जित विद्या की प्रासंगिकता की समझ,को विकसित करना,शिक्षा-कार्यक्रम का मुख्य स्तम्भ होना आवश्यक है।
विकसित देशों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अंधानुकरण घातक है क्योंकि ज़मीनी हक़ीक़त बिलकुल अलग है।इस धरती पर बैलगाड़ी भी चलती है और इसी धरती से मंगलयान भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है अर्थात गुलेल से लेकर राफ़ेल तक की पॉच हज़ार साल की सभ्यता सह-अस्तित्व में विराजमान है।अभी,कई दशकों तक,इस पूरे कालखंड की सभी आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा-दीक्षा उपलब्ध करानी है।कंप्यूटर पर,कंप्यूटर द्वारा,कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा,विकासशील देश के लिये पर्याप्त नहीं है।हर एक क्षेत्र में,देश की वर्तमान आवश्यकताओं अनुसार,हर स्तर पर,क्षैशणिक कार्य क्रम उपलब्ध होना आवश्यक है।शैक्षणिक संस्थाओं तथा उनमें शिक्षित होते हुवे छात्रों को देश की समस्याओं को समझना ही नहीं वरन,अपनी क्षमता अनुसार,उनके समाधान में सम्मिलित होना भी है।
दशकों पूर्व,विद्यालय के छात्रों की,सामाजिक कार्यों में,नियमित रूप से भागेदारी सुनिश्चित की जाती थी,उदाहरणार्थ,गाँव के मेलों में प्राथमिक उपचार शिविर लगाना,सूचना व खोजा-पाया केन्द्र संचालित करना,तथा,पेयजल-सेवा की व्यवस्था।वर्षा के मौसम में गाँवों में कुनीन की गोलियाँ बाँटना,तथा,स्वच्छता की महत्ता पर शिक्षित करना,विद्यालयों के वार्षिक कार्यक्रम माने जाते थे।यह सब,सामान्यतः,स्काउट-दल द्वारा किया जाता था,और,तब किसी भी छात्र का स्काउट होना तथा अध्यापक का स्काउट-मास्टर होना महत्व रखता था।गाँव में साक्षरता कार्यक्रम हेतु ,रात्रि विद्यालय वरिष्ठ छात्र संचालित करते थे।माना कि समय बहुत आगे चला गया है तथा समस्याओं के रूप बदल गये हैं,उनके समाधान बदल गये हैं,परंतु भारत आज भी ग्राम-प्रधान देश है तथा ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास अनिवार्य है।आज,ज्ञान-विज्ञान के आधार पर हर समस्या का हल है जिसे स्थान-विशेष की परिस्थिति के अनुरूप ढ़ालना है। ऐसे में,क्षेत्र में स्थापित महाविद्यालय,विद्यालय तथा उपलब्ध छात्र समूह की,विकास कार्यों में,क्षमता अनुसार,महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये क्योंकि उनको क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता का समुचित ज्ञान है।यह भागेदारी शिक्षा को जीवंत बनाती है,तथा, देश के भावी कर्णधारों को समाज से जोड़े रखती है।
हम आज कहॉं भटक रहे हैं यह सर्व विदित है।जब देश के प्रतिष्ठित संस्थान अपने स्नातकों की सफलता का माप- दंड उनकी तनख़्वाह को ही माने न कि उनके सामाजिक कार्य-कलाप को तो क्या कहा जाये।आज देश में शिक्षा संस्थान का मूल्याँकन,परिसर के क्षेत्रफल,रंग-रोगन तथा उपकरणों की उपलब्धता पर होता है न कि वहाँ के अध्यापकों विद्वता,उनके विशिष्ट अनुसंधान कार्य, तथा उनके सामाजिक योगदान से।
सैकड़ों बरसों से उपेक्षित,देश के आर्थिक,सामाजिक व राजनैतिक ताने-बाने के पुनर्जन्म के लिये,शैक्षिक व्यवस्था में गुणवत्ता,उपलब्धता तथा सर्व-सुलभता आवश्यक है।सीमित संसाधनों के आलोक में प्राथमिकताओं का निर्धारण अनिवार्य है तथा प्रत्येक उपकरण का अधिकाधिक उपयोग करना है।इस विशाल देश के हर शिक्षण संस्थान के हर विभाग को अपने आप में पूर्ण उपकरणयुक्त करना,न संभव है,न आवश्यक है। सर्वप्रथम हर उपकरण का,संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है क्योंकि उपयोग ही उपलब्धता की आवश्यकता दर्शाता है।
सम्पन्न देशों में,विश्वविद्यालय स्तर पर भी,संसाधन साझा किये जाते हैं।मूल्यवान संसाधनों की खरीद का औचित्य उनके यथासंभव साझा उपयोग द्वारा दर्शित होता है।खेल मैदान,सभागार,मेंहंगे उपकरण इत्यादि का विभिन्न संस्थानों द्वारा काम में लाना आम है।उदाहरणार्थ कम्प्यूटर युग के प्रारंभ में,अमेरिका में भी,एक कम्प्यूटर केन्द्र,कई विश्वविद्यालयों ने,’रिमोट जॉब ऐन्ट्री’ प्रणाली द्वारा,वर्षों तक साझा किया।कई संस्थान,जहाँ के छात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं,उनके न तो लम्बे-चौड़े परिसर हैं ,न बृहत् सभागार ,न विशाल खेल मैदान।प्राथमिकता स्पष्ट है,समर्पित शिक्षक तथा मेधावी छात्र।
दुर्भाग्यवश,देश में दिखावे की परंपरा प्रभावी रही है,तथा आज शिक्षा-क्षेत्र भी इस से अछूता नहीं रहा है।दुख इस बात का है कि नीति-निर्धारकों से लेकर नीति-अनुपालनहार तक,कहीं भी इस परंपरा के विरोध में आवाज़ नहीं उठ रही है।शिक्षा की आत्मा को समझिये,यह देश व समाज के विकास का अस्त्र है तथा इसे शानदार भवन व महँगे उपकरणों के मखमली म्यान में रख कर इसकी धार कुन्द न कीजिये।
(प्रो. एच सी पांडे, मानद कुलपति, बिट्स, मेसरा हैं)