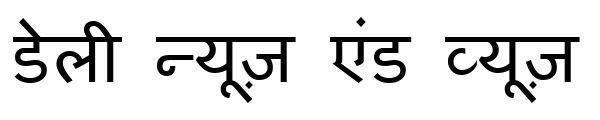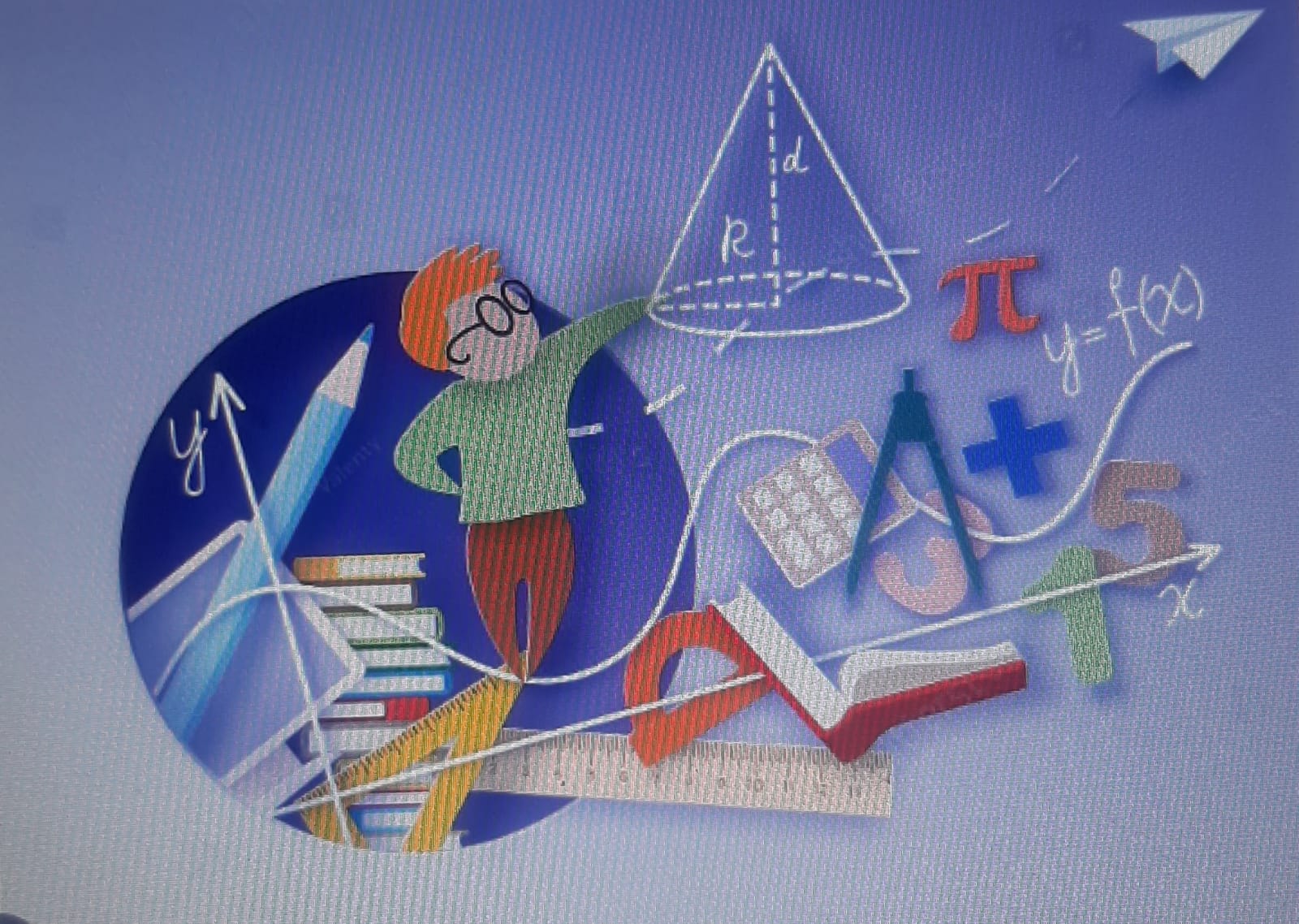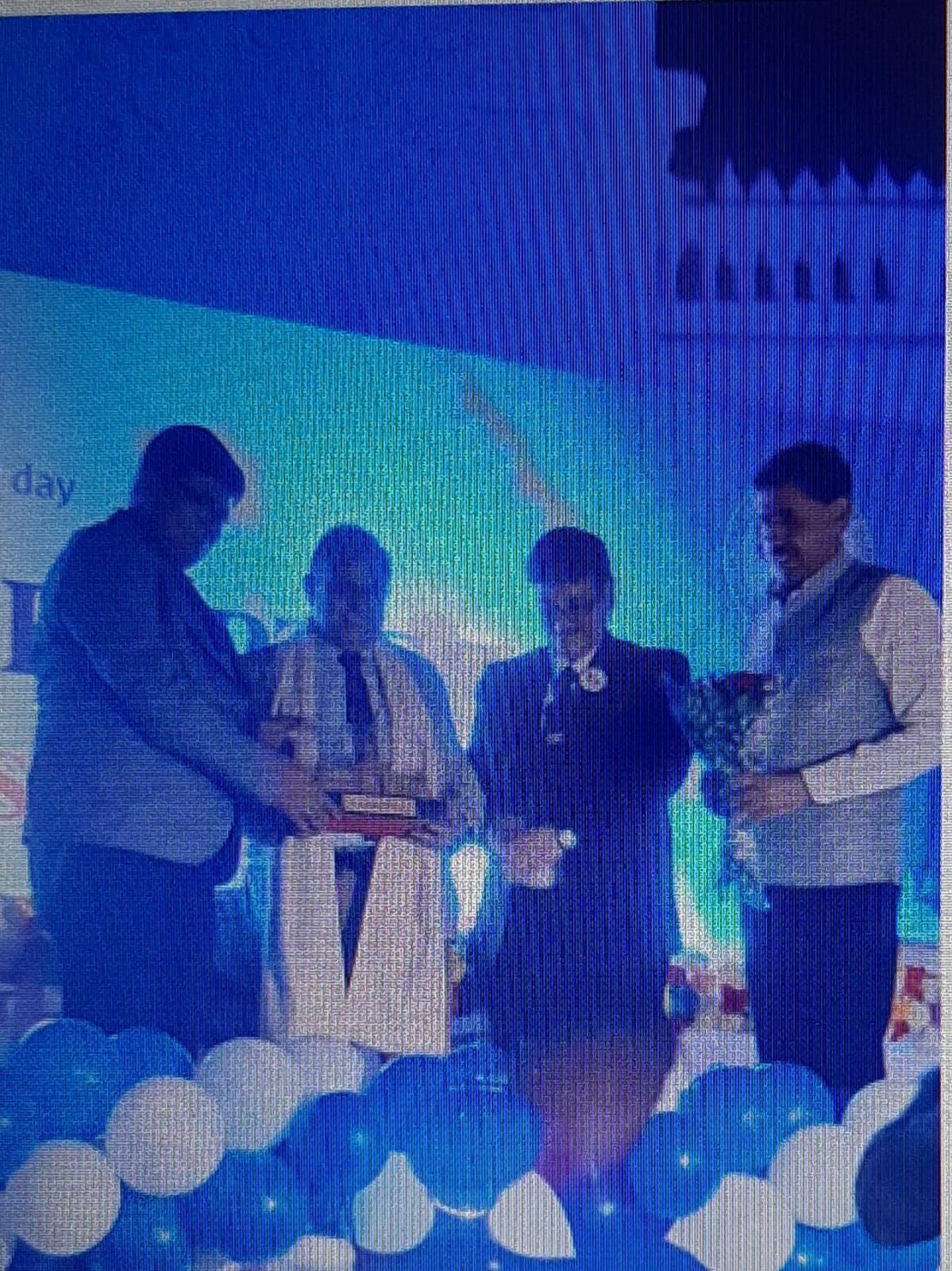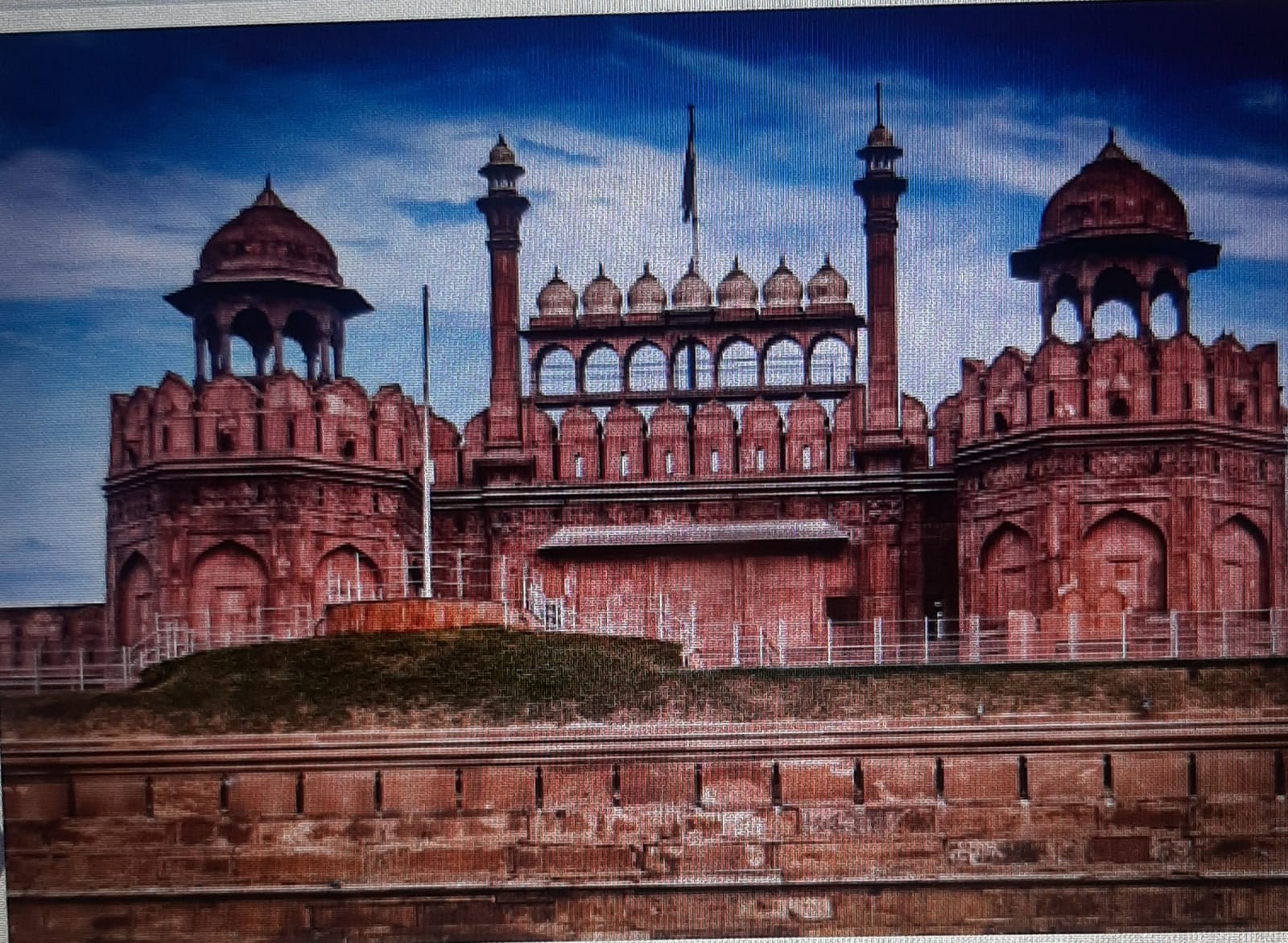प्रेम सिंह
तालाबंदी के डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी देश-व्यापी स्तर पर मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा का सिलसिला थमा नहीं है. हर दिन भूख, जिल्लत और अपने ही देश में बेगानेपन का दंश झेलते मजदूरों के हुजूम-दर-हुजूम चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं. गौर कर सकते हैं कि वे लगभग सभी युवा स्त्री-पुरुष हैं; उनके बच्चे छोटे हैं; गोद में खेलने या स्कूल जाने की उम्र वाले. काम और उसके साथ जुड़ी कमाई ठप्प होने से सभी अपने घर माता-पिता, बंधु-बांधवों के पास जाने को बेताब हैं. एक युवा भारत यह भी है, जिसकी तस्वीर देश-भर के गली-मोहल्लों-सड़कों-चौराहों-रेलवे स्टेशनों-बस अड्डों पर बिछी हुई है. गौर करने की बात यह भी है कि इस युवा भारत में हद दर्जे का साहस और जीवट है. कोरोना विषाणु ने दुनिया को मौत का दरिया बना दिया है. लेकिन इन्हें मौत का वैसा भय भय नहीं है, जैसा घरों में सुरक्षित रह सकने वालों को सता रहा है. ये पुलिस की नज़र से बच कर राजमार्गों से हट कर रास्ता लेते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल चल रहे हैं. ऐसे ही एक रास्ते पर घर वापसी करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मध्य प्रदेश के 16 प्रवासी मजदूर मालगाड़ी के नीचे कुचल कर मर गए. पहले दिन से ही यह देखा जा सकता है कि सरकार की प्रवासी अथवा निवासी मजदूरों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है. यह जानते हुए भी कि देश की 90 प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र (इनफॉर्मल सेक्टर) में हैं, वह उनसे संबंधित सूचनाओं और योजनाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करती है. ‘सावन के अंधों को सब हरा-हरा नज़र आता है’!
मजदूरों की दुर्दशा के ये साक्षात दृश्य प्रमाण हैं कि देश की ‘5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था’ में उनका पसीना ही शामिल है, वे इस अर्थव्यवस्था के हिस्सेदार नहीं हैं. असंगठित-संगठित क्षेत्र के इन मजदूरों के अलावा सीमांत किसानों, अर्द्ध-पूर्ण बेरोजगारों की भी लगभग वही स्थिति है. उन्हें तालाबंदी ने सड़कों पर तो नहीं फेंका, लेकिन रोजी-रोटी के संकट में डाल दिया है. सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि देश की अधिकांश आबादी की इस दुर्दशा से सरकार को कोई बेचैनी नहीं है. डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. जबकि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है. यानी सरकार अथवा सत्तारूढ़ पार्टी को कल चुनाव में जाना है. इस चिंताजनक परिघटना का कारण चौतरफा फैले मजदूरों की दुर्दशा के परिदृश्य में ही आसानी से पहचाना जा सकता है.
मीडिया में मजदूरों से होने वाली बातचीत के ब्यौरों से पता चलता है कि मजदूरों को अपनी इस स्थिति से कोई शिकायत नहीं है. वे इस संकट में किसी तरह घर पहुंच जाने, और तालाबंदी हटने के बाद वापस काम पर लौट आने की बात कहते हैं. वे काम न होने, रहने की जगह न होने, राशन न होने की जानकारी देते हैं, सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं करते. तालाबंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस (1 मई) भी पड़ा. हमेशा की तरह मजदूर वर्ग के गौरव और संघर्ष का स्मरण मजदूर संगठनों से लेकर सरकारों तक ने किया. लेकिन अपने मेहनतकश जीवन की सबसे बड़ी आपदा झेल रहे मजदूर अपनी पहचान से जुड़े दिवस की प्रेरणा से अछूते नज़र आते हैं. प्रगतिशील नेतृत्व जिस क्रांतिकारी श्रमिक चेतना का अत्यधिक बखान करता रहा है, उसकी अभिव्यक्त का कोई चिन्ह इन मजदूरों की बातचीत से नहीं मिलता.
भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजदूर संगठन (ट्रेड यूनियन) हैं. उनमें करीब दर्जन भर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और हजारों स्थानीय स्तर के हैं. भारत सहित पूरी दुनिया में ज्यादातर मजदूर संगठन समाजवाद, सामाजिक न्यायवाद, कल्याणवाद सरीखी प्रगतिशील विचारधाराओं से सम्बद्ध होते हैं. मजदूर संगठन मजदूरों के वेतन-बोनस, सेवा-शर्तों, काम के घंटों, काम करने की स्थितियों आदि मुद्दों पर सरकारों अथवा/और कारखाना मालिकों से संवाद, और जरूरत पड़ने पर मजदूर-वर्ग के हित में संघर्ष करते हैं. बड़े मजदूर संगठनों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम कानूनों के निर्माण/बदलाव में भी भूमिका होती है. कहने की जरूरत नहीं कि भारत का मजदूर आंदोलन लंबे समय से गतिरोध का शिकार हो चुका है. 1991 में नई आर्थिक नीतियां किसानों और मजदूरों पर सीधे-सीधे थोपी गई थीं. नई आर्थिक नीतियों के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर उसकी कीमत पर निजी क्षेत्र को स्थापित करने की शुरुआत हुई थी. वह देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था (पोलिटिकल इकॉनमी) में एक प्रतिमान विस्थापन (पेराडाइम शिफ्ट) था. सीधे शब्दों में, देश की अर्थव्यवस्था को संविधान की धुरी से उतार कर बाजार अर्थव्यवस्था (मार्केट इकॉनमी) के पुरोधा प्रतिष्ठानों – विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि) की धुरी पर चढ़ा दिया गया था. कोई भी अर्थव्यवस्था राजनीति के बाहर नहीं हो सकती. लिहाज़ा, जल्दी ही देश की राजनीति और नेतृत्व कमोबेश बाज़ार अर्थव्यवस्था का वाहक बनते चले गए.
1991 वह अवसर था जब मजदूर आंदोलन को नए चरण में प्रवेश करना चाहिए था. लेकिन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े अथवा स्वतंत्र मजदूर संगठन नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई. सरकारें ‘रिफॉर्म्स’ के नाम पर एक के बाद एक श्रम कानूनों को कारपोरेट घरानों के पक्ष में बदलती रहीं और मजदूर संगठन कुछ रस्मी प्रतिरोध करके बैठ जाते रहे. नतीजतन, भारत का मजदूर-वर्ग भी लगभग वैसा ही अराजनीतिक बनता गया है, जैसा बाकी समाज बना है. अराजनीतिकरण के चलते आधुनिक पहनावे और जीवन-शैली में लिपटा भारत का ज्यादातर पढ़ा-लिखा मध्य-वर्ग समानता के आधुनिक मूल्य को स्वीकार नहीं करता; समाज का वह हिस्सा भी नहीं, जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों के तहत मध्य-वर्ग में दाखिल हुआ है. इस परिघटना के चलते पिछले करीब तीन दशकों में देश में प्रतिक्रांति की गहरी नींव पड़ चुकी है. दुर्दशा का शिकार देश का विशाल मजदूर वर्ग उसीका नतीज़ा है. क्रांतिकारी चेतना छोड़िये, वह अपने श्रम अधिकारों के प्रति भी जागरूक नज़र नहीं आता. यह अकारण नहीं है कि आरएसएस से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) इस दौरान भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन बन कर सामने आया है.
तालाबंदी के पहले यह जरूरी था कि एक समुचित आर्थिक पैकेज के तहत मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती. सरकार ने यह नहीं किया क्योंकि उसकी प्राथमिकता मजदूर नहीं, पूंजीपति हैं. सरकार ने महामारी के बहाने करापोरेटपरस्त नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को और मजबूती से लागू करने की कमर कस ली है. उदहारण के लिए सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री का भारत को आर्थिक महाशक्ति (इकनोमिक सुपर पॉवर) बनाने का सपना साकार होगा. एक टीवी कार्यक्रम में अंबानी बंधुओं में से एक ने कहा कि विजनरी प्रधानमंत्री के रहते कोरोना महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. प्रधानमंत्री और कैबिनेट यह फैसला कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी और स्थानीय निवेश पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा. नवउदारवाद के रिसोर्स पर्सन दावे कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के बाद बनने वाली नई विश्व-व्यवस्था (वर्ल्ड आर्डर) में भारत की अग्रणी भूमिका होगी!
यह सब करने के लिए सरकार ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजदूरों पर निशाना साधा है. उसने श्रम कानूनों को और ज्यादा ‘सरल’ बनाने की कवायद शुरू कर दी है. मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक विडियो चर्चा में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने के सुझाव की प्रशसा करते हुए उसे ‘सुधारों’ (रिफॉर्म्स) की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. श्रम कानून समवर्ती सूची में आते हैं. गहलोत के सुझाव की प्रशंसा करके प्रधानमंत्री ने राज्यों को श्रम कानून कमजोर करने की अपनी मंशा संप्रेषित कर दी थी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यादेश के ज़रिये तीन सालों तक, न्यूनतम वेतन अधिनियम सहित, लगभग सभी श्रम कानूनों को अगले तीन महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा कर चुके हैं. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र की सरकारों ने भी किसी न किसी रूप में श्रम कानूनों को ढीला करने का फैसला किया है. आगे अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं. यानी अर्थव्यवस्था देश के शासक वर्ग और कारपोरेट घरानों के बीच का मामला है, मजदूर उसमें कहीं नहीं आते! (यह जरूर है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे कोरोना संकट के दौर में जो सुझाव सरकार को दिए हैं, उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि उसका नवउदारवादी अर्थव्यवस्था को मानवीय चेहरा प्रदान करने का विश्वास अभी भी बरकरार है.)
सरकार ने अपना प्रतिक्रांतिकारी चरित्र खोल कर सामने रख दिया है. वह उसी अर्थव्यवस्था की मजबूती का उद्यम कर रही है, जिसके चलते कई लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 50 करोड़ मजदूर सस्ते श्रम में तब्दील हो गए हैं. सरकार जानती है उसके सामने कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं है. मजदूर संगठनों और मजदूर नेताओं ने श्रम कानूनों में बदलाव अथवा उन्हें निरस्त करने के फैसलों का विरोध किया है. राष्ट्रीय स्तर के 10 मजदूर संगठनों ने तालाबंदी खुलने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है. यह सब जरूरी है. लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि मजदूरों की दुर्दशा के मद्देनज़र असली सवाल को चिंता और चर्चा के केंद्र में लाया जाए. असली सवाल उन आर्थिक नीतियों का है, जिनके चलते देश भर के मजदूर इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं. नवउदारवाद के समर्थक कुछ धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि राज्य सरकारों ने जो किया है वह ‘रिफॉर्म्स’ का सही अर्थ नहीं है. वे भ्रम पैदा करना चाहते हैं. नवउदारवाद में ‘रिफॉर्म्स’ का शुरुआत से एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ रहा है. उसी अर्थ के तहत 1991 के बाद से श्रम कानूनों की ताकत को मजदूर हितों के खिलाफ और कारपोरेट हितों के पक्ष में कमजोर (डाईल्युट) किया जाता रहा है. कुछ संविधानवेत्ताओं की तरफ से यह भी सुनने में आया है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों का अवमूल्यन अथवा स्थगन संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है. लेकिन वे यह नहीं कहते कि 1991 में लागू की गईं नवउदारवादी नीतियां संविधान के उलट थीं.
राजनीति को बदले बिना अर्थव्यवस्था नहीं बदली जा सकती. कोरोना महामारी को सरकार ने एक मौका बनाया है, तो मौजूदा निगम पूंजीवाद के वास्तविक विरोधी भी इसे एक मौका बना सकते हैं. मजदूरों, किसानों, अर्द्ध-पूर्ण बेरोजगारों का महामारी काल का अनुभव आसानी से भुलाने वाला नहीं होगा. उनके इस अनुभव का राजनीतिकरण होगा तो एक नई श्रमिक चेतना का उन्मेष होगा और कारपोरेट राजनीति के बरक्स वैकल्पिक राजनीति की ज़मीन बनेगी.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं)