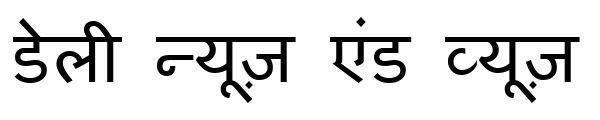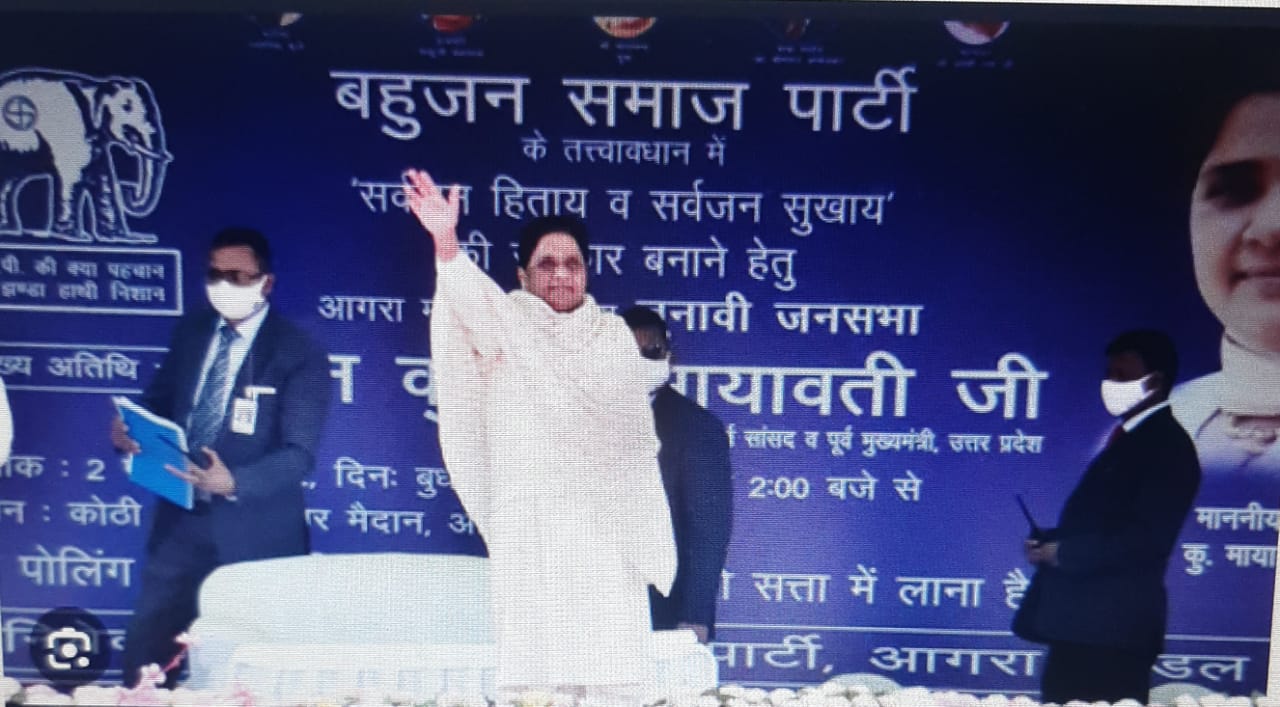एम हसन लिखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया विवाद दशकों से बहस का विषय रहा है, जहाँ दो समूह इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। यह अभी भी बहस का विषय है कि क्या “राजनीतिक इस्लाम” ने हिंदू परंपराओं को कोई नुकसान पहुँचाया है या स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में खुद को आत्मसात करके एकजुट होकर काम किया है ।
लखनऊ, 23 अक्टूबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “राजनीतिक इस्लाम” को “सनातन धर्म” के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि लोग ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद पर चर्चा करते हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक इस्लाम पर कोई चर्चा नहीं होती। दिवाली समारोह के दौरान गोरखपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जैसे लोगों के रूप में “राजनीतिक इस्लाम” फैलाने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस ने हाल ही में छांगुर को पैसे के बल पर धर्मांतरण कराने का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया विवाद दशकों से बहस का विषय रहा है, जहाँ दो समूह इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। यह अभी भी बहस का विषय है कि क्या “राजनीतिक इस्लाम” ने हिंदू परंपराओं को कोई नुकसान पहुँचाया है या स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में खुद को आत्मसात करके एकजुट होकर काम किया है।
योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी आरोप लगाया कि “राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ” विभिन्न रूपों में जारी हैं और उन्हें धर्मांतरण और आतंकवाद जैसे मुद्दों से जोड़ा। राज्य की हालिया नीति का हवाला देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, और दावा किया कि ऐसे उत्पादों से प्राप्त आय का उपयोग “धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद” के लिए किया जा रहा है।

न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों ने भी ज़ोर देकर कहा है कि राजनीतिक इस्लाम एक ऐतिहासिक और समकालीन ख़तरा है जिसका उद्देश्य भारत की जनसांख्यिकी को बदलना और उसकी आस्था को कमज़ोर करना है। हालाँकि, अकादमिक कार्यों ने इस बात का दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे इस्लाम ने भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों के लिए एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में काम किया। इसने यह भी विश्लेषण किया है कि कैसे भारत में राजनीतिक इस्लाम को स्थानीय सांस्कृतिक सीमाओं के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर किया गया। प्रति-कथात्मक रूप से, धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों ने पहचान की राजनीति में पीछे हटने के बजाय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक भविष्य की वकालत की थी।
वास्तव में, “राजनीतिक इस्लाम पर कोई चर्चा नहीं” के दावे के विपरीत, देश के विभिन्न हिस्सों के पुस्तकालयों में किताबों की अलमारियाँ लगभग सभी भाषाओं में विशाल प्रासंगिक साहित्य से भरी पड़ी हैं। सवाल यह है कि लोग इसे पढ़ते हैं या नहीं।
मुख्यमंत्री द्वारा पैदा किए गए विवाद का जिक्र करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ के संस्थापक कुलपति अनीस अंसारी ने गुरुवार को यहां कहा कि “आरएसएस-भाजपा प्रतिष्ठान इस्लाम और अल्पसंख्यकों द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य धर्मों से ग्रस्त प्रतीत होता है। राजनीतिक इस्लाम पर गलतफहमी आरएसएस-भाजपा का मुख्य आहार रहा है। बहु-धार्मिक समाज में इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म सहित किसी भी धर्म का राजनीतिकरण टाला जा सकता है। धर्म का राजनीतिक उपयोग स्वयं दुरुपयोग किए गए धर्म के अनुयायियों और पूरे देश के लिए लाभ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। अतीत में आर्यों, अरबों, फारसियों, तुर्की और ब्रिटिश राजनीतिक शासकों द्वारा धर्म के दुरुपयोग ने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाया। इस इतिहास में आरएसएस-भाजपा के वर्तमान नेताओं के लिए भी एक सबक है।
इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस बात पर अलग-अलग विचार रखे कि क्या भारत में राजनीतिक इस्लाम सनातन धर्म के लिए खतरा है। दोनों परंपराओं के बीच सदियों के जटिल अंतःक्रियाओं के आधार पर विद्वानों में आम सहमति नहीं थी, क्योंकि इस प्रश्न में ऐतिहासिक घटनाओं और समकालीन राजनीतिक गतिशीलता की विभिन्न व्याख्याएं शामिल थीं। विल डुरंट और जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने कुछ मुस्लिम आक्रमणों को हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित अभियान के रूप में चित्रित किया था, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विनाश और हिंदू संस्कृति का उन्मूलन शामिल था। इस दृष्टिकोण से, राजनीतिक इस्लाम स्वाभाविक रूप से विस्तारवादी था और इस्लामी तर्ज पर समाज का पुनर्निर्माण करना चाहता था, जिसे सनातन धर्म की बहुलवादी और विकेन्द्रीकृत प्रकृति के लिए खतरे के रूप में देखा गया था।
लेकिन ऑड्रे ट्रुश्के, रोमिला थापर और भारतीय इतिहास कांग्रेस से जुड़े अन्य धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने अधिक सूक्ष्म व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं, और तर्क दिया है कि “सभ्यताओं के टकराव” की कहानी ऐतिहासिक रूप से गलत है और आधुनिक राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। उन्होंने तर्क दिया है कि संघर्षों के बावजूद, कई मुस्लिम शासक, जिनमें अकबर प्रमुख थे, व्यावहारिक थे और उन्होंने सह-अस्तित्व, धार्मिक संरक्षण और बहुसंस्कृतिवाद की नीतियों को अपनाया। कुछ ने तो हिंदुओं को अपनी नौकरशाही और सेना में भी शामिल किया। कुछ विद्वानों ने बताया है कि इस्लामी समतावाद ने कुछ निचली जातियों के हिंदुओं को आकर्षित किया, जिसने जड़ जमाई जाति व्यवस्था को चुनौती दी, और कई धर्मांतरण केवल बल प्रयोग के बजाय सामाजिक गतिशीलता या व्यावहारिकता से प्रेरित थे।

इस्लाम के लगभग सभी मूल स्रोत अरबी और फ़ारसी में हैं, जो इस्लाम को एक धर्म और जीवन-पद्धति के रूप में जानने में एक बड़ी बाधा रहे हैं। महान लेखक प्रेमचंद ने एक बार दुःख व्यक्त किया था कि एक हज़ार साल से भी ज़्यादा समय तक एक-दूसरे के साथ रहने के बावजूद, हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत कम जानते हैं। उनका मानना था कि एक-दूसरे से अपरिचित होना भी दोनों समुदायों के बीच संदेह, वैमनस्य और सांप्रदायिक मनोवृत्ति के बढ़ने का एक प्रमुख कारण था।
महात्मा गांधी राजनीतिक इस्लाम को हिंदू-मुस्लिम एकता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ मानते थे और विभाजन के लिए इसके इस्तेमाल का विरोध करते थे। उनका मानना था कि “हृदय एकता” और राजनीतिक एकता, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और वे उस “राजनीतिक इस्लाम” को, जो भारत को विभाजित करना चाहता है, इस्लाम और भारत दोनों का दुश्मन मानते थे। गांधी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सच्चे धर्म को राजनीति को शांति, न्याय और अहिंसा की ओर ले जाना चाहिए, और मुसलमानों सहित सभी भारतीयों को भारतीय संघ के प्रति वफ़ादार होना चाहिए। गांधी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच “हृदय एकता” चाहते थे, इसे भारत की स्वतंत्रता और एक गरिमापूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि सांप्रदायिक विभाजन को अक्सर ब्रिटिश नीति और धार्मिक नेताओं द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो अपने लाभ के लिए धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाते हैं।
भारत में राजनीतिक इस्लाम पर रवींद्रनाथ टैगोर के लेखन जटिल और व्याख्या के लिए खुले हैं, सूत्रों से पता चलता है कि उनके कार्यों में सांप्रदायिकता की आलोचना और अंतर-धार्मिक समझ पर ज़ोर, दोनों परिलक्षित होते हैं। वे धार्मिक संघर्षों की संभावना और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल को लेकर चिंतित थे, खासकर जब इससे सामाजिक अन्याय या उत्पीड़न होता हो। उनका ज़ोर किसी विशिष्ट इस्लाम-विरोधी राजनीतिक रुख़ पर नहीं, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहानुभूति पैदा करने और आपसी अज्ञानता को दूर करने पर था। टैगोर ने सांप्रदायिकता से उत्पन्न होने वाले सामाजिक विभाजन और अन्याय की आलोचना की और उन्हें देश के लिए एक “अभिशाप” माना। वे धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना, समूहों द्वारा दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग को लेकर चिंतित थे। टैगोर का मानना था कि एक-दूसरे की संस्कृति और रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी का अभाव संघर्ष का एक प्रबल स्रोत है। उन्होंने समुदायों के बीच समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए विश्वभारती विश्वविद्यालय में इस्लामी संस्कृति विभाग की स्थापना करके इन विभाजनों को पाटने का प्रयास किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक इस्लाम को भारत के बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष समाज का एक घटक मानते थे, न कि एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की जब इसका इस्तेमाल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वह एक धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास करते थे जहाँ सभी धर्मों के लोग सद्भाव से रह सकें और हिंदू और मुस्लिम, दोनों तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। नेहरू धर्म के इस्तेमाल से लोगों को बाँटने के खास तौर पर खिलाफ थे और धार्मिक रूढ़िवादिता पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक सोच और तर्कवाद की वकालत करते थे। नेहरू सांप्रदायिकता के सभी रूपों, जिसमें धर्म पर आधारित कोई भी राजनीतिक लामबंदी शामिल है, के मुखर आलोचक थे और कहते थे कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था, जहाँ राज्य एक धर्म को दूसरे पर तरजीह नहीं देगा और समुदायों के बीच सद्भाव सुनिश्चित करेगा।
क्या राजनीतिक इस्लाम सनातन धर्म के लिए ख़तरा है, यह प्रश्न सरल नहीं है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। यह एक सतत और अक्सर राजनीतिक बहस है जिसकी ऐतिहासिक व्याख्या के कई स्तर हैं। ऐतिहासिक रूप से, कुछ शासकों के शासनकाल में संघर्ष और उत्पीड़न के दौर, सह-अस्तित्व, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक प्रभाव के लंबे दौर के साथ-साथ मौजूद रहे हैं। समकालीन दृष्टिकोण न केवल ऐतिहासिक घटनाओं से, बल्कि हिंदू राष्ट्रवादी और कुछ इस्लामवादी दृष्टिकोणों से आधुनिक राजनीतिक आख्यानों से भी आकार लेते हैं। इस्लाम और सनातन धर्म, दोनों ही विविध व्याख्याओं वाली जटिल परंपराएँ हैं और स्थिर, एकाकी संस्थाओं के बजाय, विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार निरंतर अनुकूलित होती रही हैं।
(एम हसन, हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ के पूर्व ब्यूरो प्रमुख हैं)