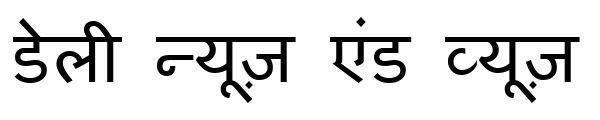एम हसन लिखते हैं कि पटना और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 13,850 किलोमीटर होने के बावजूद, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खड़े राजनीतिक दलों की राजनीतिक सोच एक जैसी है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी और बिहार में महागठबंधन के नेताओं के साथ हो रहे नस्लवादी और सांप्रदायिक दुर्व्यवहार ने साबित कर दिया है कि दुनिया भर में कट्टरता कितनी सामान्य हो गई है। लंदन के मेयर सादिक खान के साथ भी यही स्थिति है।
अगर ‘नमक हराम’, ‘बुर्का’ और ‘घुसपैठिया’ बिहार चुनावों में “इस्लामोफोबिया” पैदा करने वाले नफरत भरे कारक हैं, तो न्यूयॉर्क भी हाल ही में संपन्न हुए प्रतिष्ठित मेयर चुनाव में पीछे नहीं रहा, जिसमें एक भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम ज़ोहरान ममदानी ने अभूतपूर्व रूप से एप्पल सिटी के राजनीतिक वंश को सत्ता से बेदखल कर दिया। ममदानी का मेयर पद का चुनाव अनियंत्रित इस्लामोफोबिया से प्रभावित रहा और इसके जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। जबकि बिहार में एक कार्टून में दिखाया गया था कि “कांग्रेस की एक बस घुसपैठियों और बुर्का पहने महिला से भरी हुई चुनाव के लिए बिहार जा रही है, न्यूयॉर्क में एक कार्टून में लाल रंग के विमान जिस पर “ममदानी” लिखा था, को एक टावर की ओर जाते हुए दिखाया गया था” (आतंकवादियों द्वारा 9/11 ट्विन टावर दुर्घटना की याद दिलाते हुए)।
पटना और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी भले ही 13,850 किलोमीटर है, लेकिन एक समुदाय के खिलाफ खड़े सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक सोच एक जैसी है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी और बिहार में महागठबंधन के नेताओं को अभी भी जिस नस्लवादी और सांप्रदायिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, उसने साबित कर दिया है कि दुनिया भर में कट्टरता कितनी सामान्य हो गई है। लंदन के मेयर सादिक खान के साथ भी यही स्थिति है।
ममदानी वास्तव में नस्लवादी हमले का सामना करने वाले अकेले नहीं थे। 2008 में, तत्कालीन डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार “बराक हुसैन ओबामा” यह जानकर हैरान रह गए कि “वह मुस्लिम हैं”। ओबामा के मुस्लिम होने की अफवाहें उड़ीं, जो उनके अभियान के मीडिया कवरेज का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गईं। ओबामा के विरोधियों ने उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि पर संदेह जताया और पूछा कि अगर उन्हें पता चले कि डेमोक्रेट को हमास का समर्थन प्राप्त है तो वे कैसे वोट देंगे हालाँकि, इस मामले को सुलझाने के लिए, पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल, जो उस समय डेमोक्रेट पार्टी में शामिल हो गए थे, ने ज़ोर देकर कहा कि “ओबामा मुसलमान नहीं हैं और एक सभ्य पारिवारिक व्यक्ति हैं। वह एक ईसाई हैं। वह हमेशा से ईसाई रहे हैं।” फिर भी, पॉवेल ने आगे कहा, “अगर ओबामा मुसलमान होते तो क्या होता?” “क्या इस देश में मुसलमान होने में कोई बुराई है?”
जब उनका मध्य नाम, हुसैन, एक राजनीतिक हथियार बन गया, तो ओबामा ने खुद को इससे दूर कर लिया। “बराक ओबामा” विविधता का स्वीकार्य, भयरहित चेहरा बन गए – आकांक्षी, लेकिन सतर्क। उन्होंने शायद ही कभी अपनी मुस्लिम पृष्ठभूमि का हवाला दिया, आशा की एक व्यापक, रंगभेदी कहानी को चुना। ममदानी एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करते हैं – एक ऐसा युग जो तालमेल बिठाने में कम और दृढ़ रहने में अधिक रुचि रखता था। जब उनका मध्य नाम विरोधियों के मुंह में कलंक बन गया, तो ओबामा ने ध्यान हटा लिया। ममदानी अपना नाम तब तक धीरे-धीरे उच्चारित करते हैं जब तक कि दूसरे उसे सही नहीं बोल लेते। ओबामा मुस्लिम चश्मे से देखे जाने से बचते रहे। ममदानी कहते हैं कि मुस्लिम होना, अफ्रीका में जन्मा होना और दक्षिण एशियाई होना कहानी है – बोझ नहीं।
हालांकि, ममदानी की सफलता ने न्यूयॉर्क या कहीं और इस्लामोफोबिया को खत्म नहीं किया है अपने प्रभावशाली विजय भाषण में, न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर ने घोषणा की कि “अब न्यूयॉर्क ऐसा शहर नहीं रहेगा जहां आप इस्लामोफोबिया का लाभ उठाकर चुनाव जीत सकें।”

बिहार की बात करें तो, क्या 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में जाने वाले राज्य के मतदाता न्यूयॉर्क सिटी से कोई सबक लेंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। जैसे-जैसे बिहार में दूसरे चरण का प्रचार ज़ोर पकड़ रहा है, राजनीतिक विमर्श में एक चिंताजनक पैटर्न उभर रहा है। राज्य का राजनीतिक विमर्श नाटकीय रूप से बदल गया है। नफरत फैलाने वाले भाषण, जो कभी चुनावी बयानबाजी का एक मुख्य विषय हुआ करते थे, अब केंद्र में आ गए हैं और रैलियों, सोशल मीडिया और आधिकारिक प्रचार सामग्री के ज़रिए और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। विकास और शासन की भाषा की जगह धीरे-धीरे धर्म, जाति और “घुसपैठियों” जैसे आक्षेपों ने ले ली है, जिससे नागरिक समाज समूहों में चिंता बढ़ गई है।
नफरत पर नज़र रखने वाले एक समूह, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने हाल ही में एक रिपोर्ट में धार्मिक और जातिगत समुदायों को निशाना बनाकर नेताओं की टिप्पणियों का एक स्पष्ट पैटर्न दर्ज किया है। इसने “नमक हराम” टिप्पणी को पक्षपातपूर्ण निष्ठा के माध्यम से नागरिकता को परिभाषित करने का प्रयास बताया, एक ऐसी रेखा जो कल्याण प्राप्तकर्ताओं और राजनीतिक समर्थकों के बीच के अंतर को धुंधला कर देती है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह पैटर्न स्पष्ट है। प्रत्येक टिप्पणी संदेह के माहौल को मजबूत करती है, जहाँ पहचान ही निष्ठा निर्धारित करती है। उत्तर भारत की चुनावी राजनीति में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाने वाला “घुसपैठिया” शब्द बिहार के चुनावी जिलों में नए सिरे से प्रभावी हो गया है। और सोशल मीडिया द्वारा हर नारे को एक साझा करने योग्य मीम में बदलने के साथ, आक्रोश और प्रवर्धन का बिहार का चुनावी इतिहास जातिगत गौरव और धार्मिक विभाजन की अपीलों से भरा पड़ा है। इस बार जो बदला है, वह है प्रचार का पैमाना और गति। डिजिटल प्रचार का ढाँचा—व्हाट्सएप फ़ॉरवर्ड, एआई-जनरेटेड पोस्टर और एल्गोरिथम माइक्रो-टारगेटिंग—यह सुनिश्चित करता है कि विभाजनकारी सामग्री चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया से पहले ही तेज़ी से फैल जाए। लेकिन 14 नवंबर—जिस दिन नतीजे घोषित होंगे—ही बताएगा कि ये विभाजनकारी हथकंडे कारगर रहे या नहीं।
(एम हसन, हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ के पूर्व ब्यूरो प्रमुख हैं)